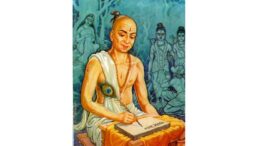भारत को इसके 5 हस्तशिल्प के माध्यम से देखें
भारत को हमेशा अपनी पारंपरिक कला और शिल्प के माध्यम से सांस्कृतिक और पारंपरिक जीवंतता को दर्शाने वाली भूमि के रूप में जाना जाता था। यहां के हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की अपनी अलग सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान है जो इसके हस्तशिल्प में झलकती है।
हम आपके लिए लाए हैं भारत की ऐसी ही पांच कलाएं और उनकी कहानियां।
1- ज़रदोज़ी, लखनऊ
लखनऊ चिकनकारी और ज़रदोज़ी दस्तकारी के लिये मशहूर है। यहां मुग़ल शासकों के दौर में इस शाही कला को बहुत बढ़ावा मिलता था। मुग़लों के बाद अवध के नवाबों ने भी इसे बहुत संरक्षण दिया। ज़रदोज़ी के कारीगर दूसरी जगहों से लखनऊ के दरबारों में आये थे और इस तरह बहुत जल्द ज़रदोज़ी के काम वाले लिबास नवाबों के परिधानों का हिस्सा बन गए। नवाब शुजाउद्दौला (1754- 1775) ने इस दस्तकारी में बहुत दिलचस्पी दिखाई थी। उन्होंने इस कला को संरक्षण दिया और कारीगरों को इनाम में ज़मीनें भी दी गई थीं जिसकी वजह से उत्तर भारत के अन्य ज़रदोज़ी केंद्रों की तुलना में लखनऊ ज़्यादा मशहूर हो गया। इसके बाद नवाब वाजिद अली शाह (1846-56) ने इस कला को आगे बढ़ाया और इस तरह ये कला भी चिकनकारी की तरह लखनऊ की पहचान बन गई।
अंग्रेज़ सैनिक अधिकारी सर विलियम बर्डवुड के अनुसार नवाब अपने लिबास पर ख़ास ध्यान देते थे और यही पहनावे में उनकी दिलचस्पी की वजह भी थी। अवध के नवाबों के कई चित्रों में उनके पहनावे पर ज़रदोज़ी का काम देखा जा सकता है। ये कला लखनऊ के राज्य संग्रहालय, लखनऊ अमीरउद्दौला लाइब्रेरी और लखनऊ हॉल तालुक़दार में आज भी अच्छे से संरक्षित है। ज़रदोज़ी का काम सिर्फ़ नवाबों और उनके अमीरों (स्त्री-पुरुष दोनों) के लिबासों पर ही नहीं बल्कि उनकी टोपियों और जूतियों पर भी होता था। उस ज़माने के, उर्दू के बड़े लेखक अब्दुल हलीम शरर ने कई जूतियों के नाम गिनाए हैं जैसे ख़ुर्दनोक(छोटी नोक), चरवन, आरामपाई, कोंश, ज़रपाई, ज़ुफ़्तपाई, सलीम शाही, बूट और पेशावरी। शरर ने ये भी बताया कि हुक़्क़े की नली पर भी ज़रदोज़ी का काम होता था। सर्दियों के दिनों में ज़रोदज़ी के काम वाली पश्मीना शॉलों की बहुत मांग होती थी। और पढ़ें
2 – इकत, गुजरात
गुजरात में बनने वाला पटोला भारत में सबसे मशहूर इकत है। पारम्परिक तौर से पटोला राजकोट और पाटन में बुना जाता है। लेकिन पाटन के सिल्क का पटोला ख़ास है क्योंकि ये डबल इकत शैली में होता है। पाटन की रानी की वाव की शिल्पकारी में भी पटोला कपड़े के नमूने देखे जा सकते हैं।
पाटन का पटोला साल्वी समुदाय बुनता है जो महाराष्ट्र और कर्नाटक से यहां आए थे। किवदंतियों के अनुसार 12वीं शताब्दी में सोलंकी सम्राट कुमारपाला ने पूजा के लिए सिल्क का ख़ास कपड़ा बनवाने के लिए जालना से साल्वी समुदाय के बुनकरों को बुलवाया था। कहा जाता है कि राजा ये कपड़ा सिर्फ़ एक बार पहनता था फिर उसे दान कर दिया जाता था या फिर बेच दिया जाता था।
पाटन पटोला ज्यामितीय पैटर्न, फूलों का रूपांकन और सुंदर डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। डबल इकत वाली पटोला साड़ी बनाने में बहुत समय भी लगता है और यह एक बहुत मेहनत का काम है। इस साड़ी को बनाने के 25 चरण तक हो सकते हैं जो की रंगों की संख्या पर निर्भर करता हैं।एक साड़ी बनाने में एक साल भी लग सकता है और ये बहुत महंगी भी होती है। कभी कभी तो धागों को रंगने में ही 75 दिन तक लग जाते हैं। और पढ़ें
3- बिदरी, कर्नाटक
चांदी, सोने, कांसे और धातु पर क़लमकारी के लिए मशहूर बीदर धातुकला भारतीय धातुकला का एक प्राचीन रुप है। इसका नाम बहमनी सुल्तानों की राजधानी बीदर के ही नाम पर पड़ा है। इस धातुकला में फ़ारसी, तुर्की और इस्लामिक संस्कृति की झलक मिलती है। बिदरी धातुकला 14वीं शताब्दी की है और इसका संबंध उस जगह से है जहां बीदर क़िला है।
ऐसा माना जाता है कि ईरान के प्रसिद्ध शिल्पी अब्दुल्लाह बिन क़ैसर को सुल्तान अहमद शाह बहमनी (1422-1436) ने बीदर के शाही महलों और दरबारों को सजाने के लिये बुलाया था। इस काम के लिये अब्दुल्लाह ने एक स्थानीय सुनार की मदद ली और यहीं से बिदरी धातुकला का जन्म हुआ। सुल्तान अहमद शाह बहमनी के शासनकाल के दौरान बीदर विश्व के धातु कलाकारों पीढ़ियों तक बिदरी धातुकला बीदर और बाद में हैदराबाद के लोगों के लिये रोज़गार का ज़रिया रही है जहां आज भी कला की ये धरोहर जीवित है।
बिदरी धातुकला में बहुत कौशल की ज़रुत होती है और समय भी बहुत लगता है। बिदरी धातुकला से किसी धातु को रुप देने में आठ चरणों से गुज़रना होता है। पहले चरण में धातु को वैसा रुप दिया जाता है जैसी चीज़ बनाना है, जैसे बर्तन या डिब्बा। इसके बाद इसे चिकना किया जाता है और फिर छेनी से इस पर आकृति तराशी जाती है। आकृति जितनी पेचीदा होगी, उसी अनुसार इसमें समय लग सकता है। इसके बाद शुद्ध चांदी की चादर या तारों पर जड़ाई का काम होता है। इसके बाद फिर इसे चिकना किया जाता है। अंतिम चरण में काले रंग का प्रयोग किया जाता है। दिलचस्प बात ये है कि बिदरी धातुकला के कारीगर इसे बनाने में अम्लीय मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं जो सिर्फ़ बीदर क़िले में ही मिलती है। ये मिट्टी बिदर में बनने वाली वस्तुओं के ऑक्सीकरण के लिये ज़रुरी होती है। इससे वस्तू को एक ख़ास तरह का काला रंग मिलता है। ये पूरी प्रक्रिया हाथों से ही की जाती है। और पढ़ें
4- पट्टचित्र, ओडिशा
ओडिशा में पट्टचित्र कला से कई लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं और इनका पुरी के भगवान जगन्नाथ से गहरा संबंध है जो कृष्ण के अवतार थे। ज्येष्ठ माह में (मई-जून) की पूर्णिमा पर जगन्नाथ के देवताओं को गर्मी से बचाने के लिये स्नान के लिये ले जाया जाता है। माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ का जन्म हुआ था। ये वो दिन है जब हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान-यात्रा में शामिल होते हैं। इस पवित्र यात्रा में जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई भालभद्र की मूर्तियों को स्नान के लिये ले जाया जाता है। माना जाता है कि स्नान की वजह से देवी-दोवता जुलाई में आषाण (जून-जुलाई) के पहले पखवाड़े में पन्द्रह दिन के लिये बीमार हो जाते हैं।
पट का अर्थ कपड़ा होता है जबकि चित्र का मतलब पेंटिंग है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर संस्कृत है, पट्टचित्र पारंपरिक रुप से कपड़े पर बनाई जाती है जिसे आसानी से लपेटा जा सकता है। पट्ट कपड़े, अमूमन पुरानी साड़ियों से बनाया जाता है जिन पर कलफ़ न लगा हो। इन कपड़ों को इमली के बीज से बनाए गए पेस्ट से जोड़ा जाता है। ये पेस्ट बनाने के पहले इमली के बीज को 2-3 दिन तक भिगोकर रखना होता है और इसके बाद ही इसे पीसकर पेस्ट बनाया जाता है जो चिपचिपा होता है। कपड़े को चिपकाने वाले इस गोंद का पारंपरिक नाम नीर्यास कल्प है। कपड़ों की और तहों को चिपकाने के लिये इमली के बीज के साथ कैथा या बेल के रस का भी प्रयोग किया जाता है। वांछित मोटाई मिलने पर कपड़े को धूप में सुखाया जाता है और इस तरह पट्ट तैयार हो जाता है। और पढ़ें
5- टेराकोट, राजस्थान
राजस्थान के राजसमंद ज़िले में उदयपुर से क़रीब 50 कि.मी. दूर स्थित है एक छोटा सा गांव मोलेला। पहली नज़र में गांव में ऐसी कोई ख़ास बात नज़र नहीं आती है लेकिन ग़ौर से देखने पर पता चलता है कि ये गांव कोई मामूली गांव नहीं है और ये देश में टेराकोट की परंपरा का गढ़ रहा है।
मोलेला में टेराकोटे का काम पारंपरिक रुप से कुम्हार समुदाय करता है जिनके अमूमन नाम प्रजापत या प्रजापति होते हैं। कुम्हार समुदाय का विश्वास है कि ये कला उनके पुरखों को भगवान देवनारायण ने सिखाई थी जो नैत्रहीन थे। माना जाता है कि भगवान देवनारायण ने, इनके पुरखे के सपने में आकर उन्हें ये कला सिखाई थी।
मोलेला टेराकोटा आयताकार प्लेटें होती हैं जो मिट्टी से बनाई जाती हैं। इन्हें बनाने के बाद उच्च तापमान पर पकाया जाता है। इन प्लेटों पर देवी-देवताओं, ख़ासकार लोक और आदीवासी परंपरा से संबंधित देवी-देवताओं की तस्वीरें अंकित होती हैं। इन देवी-देवताओं का भील, गुज्जर और जाट जैसे लोक तथा आदिवासी समुदायों में ख़ास महत्व है। मोलेला के टेराकोट ने इन तमाम समुदायों को एक घागे में पिरो दिया है क्योंकि ये सभी इन देवी-देवताओं की उपासना करते हैं। इन समुदायों के धार्मिक और सामाजिक जीवन का इस टेराकोट कला से गहरा नाता है। और पढ़ें
हम आपसे सुनने को उत्सुक हैं!
लिव हिस्ट्री इंडिया इस देश की अनमोल धरोहर की यादों को ताज़ा करने का एक प्रयत्न हैं। हम आपके विचारों और सुझावों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ किसी भी तरह से जुड़े रहने के लिए यहाँ संपर्क कीजिये: contactus@livehistoryindia.com