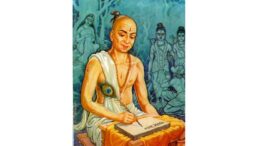ज़रदोज़ी: लखनऊ की शाही कला
शुद्ध सोने से लिपटे बदन से ज़्यादा और राजसी ठाट क्या हो सकता है? लेकिन इस राजसी शान को बरसों पहले ज़रदोज़ी ने संभव बना बना दिया था। कपड़ों पर सोने और चांदी की ज़रदोज़ी की पारंपरिक कशीदाकारी का काम भारत में मुग़लकाल में पनपा था। तब सिर से पैरों तक पहने जाने वाले पारंपरिक ज़रदोज़ी वाले लिबास शाही लोगों की शान हुआ करते थे। ये एक समय समृद्धी का प्रतीक हुआ करती थे। ये काम शाही साज़-ओ- सामान, आफ़ताबगीरों (छतरियों) और घुड़सवारों की साजसज्जा पर भी होता था।
लेकिन ये शिल्पकला इससे भी कहीं पुरानी है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता (दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर पांचवीं सदी ) की गुफाओं की चित्रकारी में ज़रदोज़ी का काम देखा जा सकता है। लेकिन इसका आरंभिक उल्लेख वेदिक युग के ग्रंथों में भी मिलता है। वाल्मिकी रचित रामायण में भी सोने के घागे से ज़रदोज़ी के काम के कई सबूत मिलते हैं। रामायण में सोने और चांदी के ज़रदोज़ी वाले महाराजवस्त्रों का उल्लेख है। गुरुद्वारों, कुछ मंदिरों और मक्का (काबे) की दीवारों पर ज़रदोज़ी का काम देखा जा सकता है।
इस शिल्पकला का संबंध ईरान से भी रहा है। ज़रदोज़ी शब्द फ़ारसी के दो शब्दों को मिलाकर बना है। ज़र का मतलब होता है सोना और दोज़ी का मतलब होता है कशीदाकारी। भारत में हाथ से की जाने वाली कशीदाकारी उस समय फलीफूली थी जब सल्तनतें (13वी-16वीं शताब्दी) हुआ करती थीं। लेकिन मुग़लकाल में ये ज़्यादा पनपी। मुग़लकाल में आगरा और दिल्ली में ज़रदोज़ी कशीदाकारी बहुत लोकप्रिय हो गई थी और तभी ईरान और फ़ारस से ये काम करने वाले शिल्पी आगरा और दिल्ली जैसे शहरों में आकर बस गए थे। मुग़लकाल के शाही दरबारों के लघुचित्रों में राजसी परिधानों पर सोने के फूलों के रुपांकनों की महीन कशीदाकारी देखी जा सकती है। बादशाह जहांगीर के शासनकाल में उनके संस्मरणों तुज़ुक-ए-जहांगीरी में शाही लिबासों पर सोने की कढ़ाई का उल्लेख है। जहांगीर की पत्नी नूरजहां भी इस शिल्पकला की बड़ी संरक्षक थीं और यही वो समय था जब ज़रदोज़ी शिल्पकला ने भारत में अपनी ख़ास जगह बनाई।
मुग़लकाल में ज़रदोज़ी को शाही काम कहा जाता था और 16वीं शताब्दी में मुग़ल बादशाह अकबर के संरक्षण में ये कला सबसे ज़्यादा फलीफूली लेकिन 17वीं शताब्दी में बादशाह औरंगज़ेब के शासनकाल में इस कला का पतन होने लगा क्योंकि इसे शाही संरक्षण मिलना बंद हो गया था। इस कला के और बुरे दिन 18वीं शताब्दी में तब शुरु हो गए जब इससे जुड़े कारीगर देश के दूसरे हिस्सों में जाकर बसने लगे। ज़रदोज़ी का काम कराने वालों को ज़रदोज़न कहते हैं जिन्हें ये कला विरासत में मिली है। कशीदाकारी की ये समृद्ध और शानदार शिल्पकला दौलंतमंद हिंदुओं, मुसलमानों और यूरोपीय लोगों की वजह से हैदराबाद, कलकत्ता, वाराणसी, अजमेर, भोपाल, कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली, सूरत और चेन्नई जैसे केंद्रों में ख़ूब फलीफूली।
मुग़लकाल के अंतिम वर्षों में संरक्षण के अभाव और महंगे कच्चे माल की वजह से इस पारंपरिक कला के उत्पादों की मांग कम होने लगी। इस कला से जुड़े कारीगर रोज़गार की तलाश में दिल्ली छोड़कर राजस्थान और पंजाब के दरबारों में चले गए। 19वीं शताब्दी में अन्य कलाओं की तरह ज़रदोज़ी पर भी औद्योगीकरण की मार पड़ी।
सन 1947 में आज़ादी मिलने के फ़ौरन बाद भारत सरकार ने न्यूनतम मज़दूरी और कौशल विकास जैसे कार्यक्रमों के ज़रिये ज़रदोज़ी से जुड़े कारीगरों को बढ़ावा देने की दिशा में क़दम उठाए।
ज़रदोज़ी क्या है?
पारंपरिक और ऐतिहासिक रुप से ज़रदोज़ी के काम में क़ीमती नगों और हीरों के साथ सिर्फ़ सोने और चांदी के तारों का इस्तेमाल होता था। लेकिन समय के साथ इनकी जगह रेशम और दबक्का (सोने और रेशम मिश्रित धागा), कसाब ( चांदी अथवा धातु के मुलम्मे वाला धागा) और बुलियन (तांबे और पीतल के मुलम्मे वाला धागा) जैसे अन्य महीन धागों ने ले ली। क़ीमती नगों की जगह सलमा-सितारों अथवा धातु के सितारों, चमकीले गोल कांचों, कांच तथा प्लास्टिक के मनकों का इस्तेमाल होने लगा है। इस सब के बावजूद कढ़ाई की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ज़रदोज़ी में अब महीन रेशम, साटन, मख़मल और बेलबूटेदार कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। कपड़ों. साज़ सामान आदि पर जब ज़रदोज़ी के काम के पैटर्न देखते ही बनते हैं।
ज़रदोज़ी के दो रुप होते हैं कारचोबी और कामदानी। कारचोबी ज़रदोज़ी मख़मल और साटन जैसे मोटे कपड़ों की जाती है। करचोबी ज़रदोज़ी का काम अमूमन जैकट, टेंट, साज सामानों और शामियानों पर किया जाता है। कामदानी ज़रदोज़ी बहुत नाज़ुक होती है। इसका काम रेशम और मलमल जैसे क़ीमती कपड़ों पर किया जाता है। दुपट्टे और नक़ाब के लिये इसे सबसे उपयुक्त माना जाता है। राजस्थान को कामदानी ज़रदोज़ी के लिये जाना जाता है।
कैसे होता है ज़रदोज़ी का काम
ज़रदोज़ी का काम कारीगर लकड़ी के अड्डे के सामने ज़मीन पर एक पांव पर, दूसरे पांव को रखकर शुरु करते हैं। ज़रदोज़ी शिल्पकला में डिज़ाइन बहुत विस्तृत और पेचीदा होती है इसलिये कढ़ाई का एक पीस तैयार करने में कई कारीगरों की ज़रुरत पड़ती है। एक अड्डे पर पांच से सात कारीगर काम कर सकते हैं और हर कारीगर के पास औज़ार होते हैं जिनका वह आसाननी से उपयोग कर सकते हैं
औज़ारों में मुड़े हुए हुक, सुई, सलमा (सोने के तार), सितारे (धातु के सितारे), गोल कांच, कांच और प्लास्टिक के मनके, डबका (एक तरह का धागा) और कसब (एक अन्य तरह का धागा) शामिल हैं। कढ़ाई में इस्तमाल होने वाली क्रोशिये की तरह की सुई लकड़ी की एक डंडी से बंधी रहती है जिसके सिरे पर एक हुक लगा रहता है। इस सुई को आरी कहते हैं और इसीलिये कढ़ाई को आरी का काम भी कहा जाता है।
• डिज़ाइन-अड्डे पर कपड़ा फैलाने और काम शुरु होने के पहले वो डिज़ाइन बनाई जाती है जिसकी कढ़ाई होनी है। अक्सी कागज़ (ट्रेसिंग पेपर) पर पहले डिज़ाइन बनाई जाती है। इसके बाद ट्रेस लाइन के साथ एक सुई से कागज़ पर छेद किए जाते हैं। मुग़लकाल में डिज़ाइन जटिल हुआ करती थीं। ये डिज़ाइन फूल और पत्तियों के रुपांकन होते थे। आज के ज़माने में डिज़ाइन और पैटर्न ज़्यादातर ज्यामितीय आकार के होते हैं।
• ट्रेसिंग- अगली प्रक्रिया में मेज़ पर बिछे रेशम, साटन या फिर मख़मल के कपड़े पर अक्सी कागज़ रखा जाता है जिस पर रुपांकन बने होते हैं। इसके बाद मिट्टी के तेल और स्याही का घोल बनाकर उसमें कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को डुबोया जाता है। इसके बाद कपड़ों के इन टुकड़ों को अक्सी कागज़ पर रगड़ा जाता है। इस प्रक्रिया से छेदों के ज़रिये कपड़े पर डिज़ाइन उभर आती है।
इसके बाद सुई के ज़रिये ज़रदोज़ी के हर अंश को बाहर खींचा जाता है और कपड़े में सुई डालकर इन अंशों को मूल डिज़ाइन में समाहित कर लिया जाता है। ज़रदोज़ी के सबसे महंगे और चमकीले उदाहरणों में कम क़ीमत वाले मोती और नग का काम शामिल है।
• कढ़ाई- कढ़ाई की प्रक्रिया के लिये लकड़ी की छड़ी, जिसे आरी कहते हैं, पर बंधी क्रोशिये जैसी सुई का इस्तेमाल होता है। आरी की वजह से काम तेज़ी से होता है क्योंकि इसकी मदद से कारीगर कपड़े के ऊपर और नीचे धागों को आसानी से इधर से उधर कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में काम पूरा करने में कितना समय लगेगा ये डिज़ाइन और इस काम पर लगे कारीगरों की संख्या पर निर्भर करता है। वैसे इस काम में एक से दस दिन लग जाते हैं।
लखनऊ की ज़रदोज़ी
लखनऊ, चिकनकारी और ज़रदोज़ी दस्तकारी के लिये मशहूर है। यहां मुग़ल शासकों के दौर में इस शाही कला को बहुत बढ़ावा मिलता था। मुग़लों के बाद अवध के नवाबों ने भी इस बहुत संरक्षण दिया। ज़रदोज़ी के कारीगर दूसरी जगहों से लखनऊ के दरबारों में आये थे और इस तरह बहुत जल्द ज़रदोज़ी के काम वाले लिबास नवाबों के परिधानों का हिस्सा बन गए। नवाब शुजाउद्दौला (1754-26 जनवरी 1775) ने इस दस्तकारी में बहुत दिलचस्पी दिखाई थी। उन्होंने इस कला को संरक्षण दिया और कारीगरों को इनाम में ज़मीनें भी दी गई थीं जिसकी वजह से उत्तर भारत के अन्य ज़रदोज़ी केंद्रों की तुलना में लखनऊ ज़्यादा मशहूर हो गया। इसके बाद नवाब वाजिद अली शाह (1846-56) ने इस कला को आगे बढ़ाया और इस तरह ये कला भी चिकनकारी की तरह लखनऊ की पहचान बन गई।
अंग्रेज़ सैनिक अधिकारी सर विलियम बर्डवुड के अनुसार नवाब अपने लिबास पर ख़ास ध्यान देते थे और यही पहनावे में उनकी दिलचस्पी की वजह भी थी। अवध के नवाबों के कई चित्रों में उनके पहनावे पर ज़रदोज़ी का काम देखा जा सकता है। ये कला लखनऊ के राज्य संग्रहालय, लखनऊ अमीरउद्दौला लाइब्रेरी और लखनऊ हॉल तालुक़दार में आज भी अच्छे से संरक्षित है। ज़रदोज़ी का काम सिर्फ़ नवाबों और उनके अमीरों (स्त्री-पुरुष दोनों) के लिबासों पर ही नहीं बल्कि उनकी टोपियों और जूतियों पर भी होता था। उस ज़माने के, उर्दू के बड़े लेखक अब्दुल हलीम शरर ने कई जूतियों के नाम गिनाए हैं जैसे ख़ुर्दनोक(छोटी नोक), चरवन, आरामपाई, कोंश, ज़रपाई, ज़ुफ़्तपाई, सलीम शाही, बूट और पेशावरी। शरर ने ये भी बताया कि हुक़्क़े की नली पर भी ज़रदोज़ी का काम होता था। सर्दियों के दिनों में ज़रोदज़ी के काम वाली पश्मीना शॉलों की बहुत मांग होती थी।
लखनऊ में ज़रदोज़ी के कारख़ाने पुराने मोहल्लों या कश्मीरी मोहल्ला और सआदतगंज जैसे इलाक़ों में स्थित हैं। यहां की आबादी में ज़्यादातर शिया मुस्लिम कारीगर हैं जो शहर के बाज़ारों में ज़रदोज़ी के काम वाले कपड़ों की सप्लाई करते हैं। कारख़ाने के मालिक करख़नदार होते हैं जो कारीगरों को काम देते हैं। करख़नदार की देखरेख में ही ज़रदोज़ी का काम होता है। पुराने शहर और पास के गांवों में कई परिवार पुश्तों से इस काम में लगे हुए हैं।
आरी और ज़रदोज़ी हालंकि एक ही कला के हिस्से हैं लेकिन इनकी तकनीक अलग अलग है। जैसे आरी में लकड़ी की सुई, जो पेंसिल की तरह होती है, कपड़े पर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चलती है जबकि ज़रदोज़ी में सुई दाएं से बाएं और बाएं से दाएं चलती है।
ज़री का धागा बनाने के लिये सोने और चांदी के मिश्रधातु का इस्तेमाल किया जाता है। ये नाज़ुक तार पिघले शिलिका का बना होता है। इन शिलिकाओं को स्टील की छेद वाली चादरों से दबाकर निकाला जाता है। इससे बनने वाले धागे को फिर हथोड़ी से और चपटा किया जाता है और तब कहीं जाकर धागा तैयार होता है। भट्टी से निकालने के बाद इन धागों को रेशम पर लपेटा जाता है।
सन 2013 में लखनऊ ज़रदोज़ी को प्रतिष्ठित जीआई (Geographical Indications) टैग मिला था। इस तरह सदियों पुरानी ज़रदोज़ी कला को आधिकारिक मान्यता मिली। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के अनुसार लखनऊ में ज़रदोज़ी उत्पाद बनाने वाले दस हज़ार से ज़्यादा लघु और छोटे उद्योग हैं। पहले इस तरह की कढ़ाई का काम पुरुष ही किया करते थे लेकिन अब इस काम में लगे कारीगरों में पंद्रह प्रतिशत महिलाएं भी हैं।
आज ज़रदोज़ी
आज ज़रदोज़ी के काम वाले महंगे उत्पाद फ़ैशन में हैं जिनकी सारी दुनिया में मांग है। यूरोपीय फ़ैशन शो के रैंप पर ज़रदोज़ी के काम वाले उत्पाद नज़र आते हैं। वक़्त के साथ बने रहने के लिये अब ज़रदोज़ी का काम साड़ियों और लहंगों तक ही सिमट कर नहीं रह गया है। अब तकियों के कवर, पर्दों, जैकट, पर्स, बेल्ट, शॉल और जूतों-जूतियों पर भी ज़रदोज़ी का काम होता है। इन उत्पादों का अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्व देशों में निर्यात होता है।
लेकिन भारत में अन्य कई पारंपरिक कलाओं की तरह ज़रदोज़ी के अस्तित्व पर भी ख़तरे के बादल मंडरा रहे हैं। इस कला के सुनहरे दिनों के बाद से फ़ैशन में कई बदलाव हो चुके हैं। अब लोग पारंपरिक डिज़ाइन और कपड़े की जगह समकालीन डिज़ाइन और आधुनिक कपड़ों को चुनना पसंद करते हैं।
इसके अलावा सोने और चांदी के भाव भी आसमान छूने लगे हैं जिससे इस कला के लिये ज़रुरी कच्चा माल बनाया जाता है। महंगे सोने चांदी की वजह से ज़रदोज़ी के उत्पाद ज़्यादातर लोगों की पहुंच के बाहर हैं। लेकिन सस्ते विकल्प भी हैं। इन विकल्पों वाले उत्पादों में सोने और चांदी के धागों की जगह तांबे और पीतल के तारों से कढ़ाई की जा रही हैं जिन पर सोने का मुलम्मा चढ़ा होता है। अगर ये भी आपको महंगा लगता है तो फिर सिंथेटिक ज़रदोज़ी के भी उत्पाद हैं जो न सिर्फ़ बहुत सस्ते होते हैं बल्कि चलते भी ख़ूब हैं।
क़रीब तीन दशक पहले मशीनों के आ जाने से इस कला का हुलिया ही बदल गया और इसकी पारंपरिक चमक और फीकी पड़ गई। ज़रदोज़नों का कहना है कि एक ज़माने में ये शाही पेशा होता था लेकिन अब कारख़ानों, फ़ैशन डिज़ाइनरों और इसे बेचने वालों के लिये ये बस पैसा कमाने का धंधा बनकर रह गया है। ये लोग ज़रदोज़नों को बहुत कम मेहनताना देते हैं। नतीजे में कई कारीगर ये काम छोड़ चुके हैं और नयी पीढ़ी ने भी इस काम से दूरी बना ली है। बदक़िस्मती से ज़रदोज़ी की ये शानदार कला विलुप्त होने की कगार पर खड़ी है।
हम आपसे सुनने को उत्सुक हैं!
लिव हिस्ट्री इंडिया इस देश की अनमोल धरोहर की यादों को ताज़ा करने का एक प्रयत्न हैं। हम आपके विचारों और सुझावों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ किसी भी तरह से जुड़े रहने के लिए यहाँ संपर्क कीजिये: contactus@livehistoryindia.com